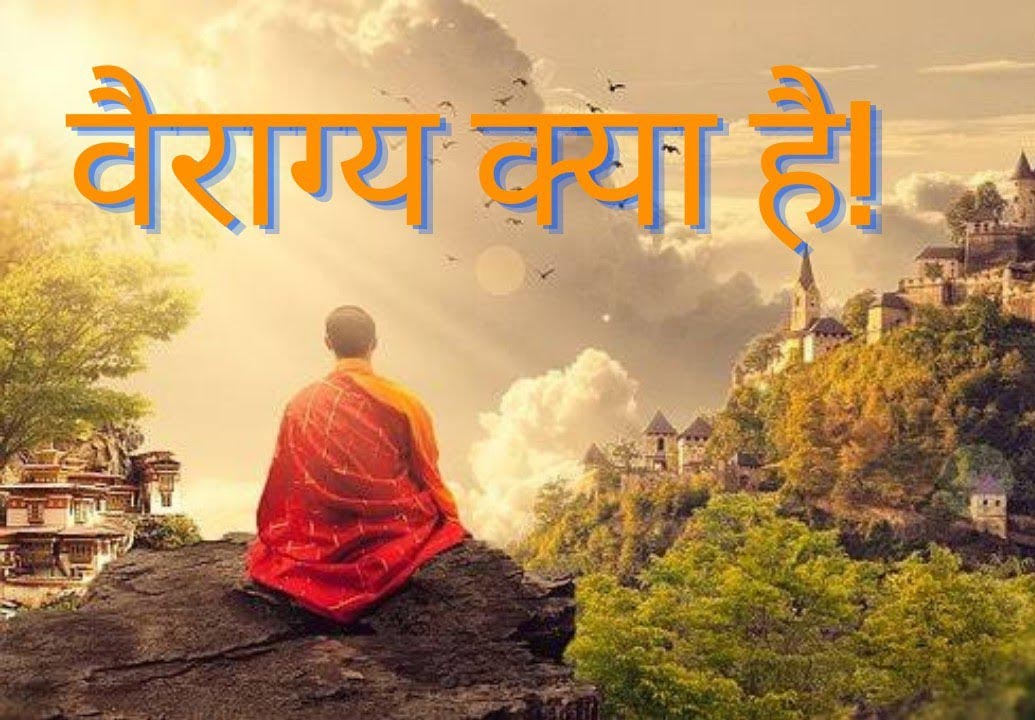भगवद् गीता अध्याय 6 श्लोक 35
श्री भगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं.
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते..
अर्थात
श्रीभगवान् कहते हैं – हे, महबाहो निसन्देह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है. परन्तु, हे कुन्तीपुत्र उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है.
वैराग्य, हिन्दू, बौद्ध तथा जैन आदि दर्शनों में प्रचलित प्रसिद्ध अवधारणा है. वैराग्य मन की वह वृत्ति है, जिसके कारण संसार की विषय वासना तुच्छ प्रतीत होती है और व्यक्ति संसार के झंझट छोड़कर एकांत में रहता है और ईश्वर का भजन करता है. घर-बार छोड़कर हरिद्वार जाकर बैठ जाने का नाम वैराग्य नहीं है. तो वैराग्य क्या है? संसार को असार जानना, देह को मिट्टी समझना – वैराग्य है. उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि तुम शहर या गांव में रहो या हिमालय की किसी गुफा में रहो. अगर आपको यह बात समझ आ गई कि आपकी यह देह मिट्टी है और जिस संसार को आप देख रहे हो, यह सदा नहीं रहेगा, इस बात का निश्चय हो जाए, यही वैराग्य है.
महर्षि पतंजलि कहते हैं –
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं
मन, पांच इन्द्रियों के विषय वस्तुओं से बने इस संसार की ओर भागता रहता है. तुम यदि शांत बैठे हो, चाहे तो आंखें खुली हों या बंद, देखो तुम्हारा मन कहां जाता है. तुम्हारा मन कुछ देखने के लिए भागता है, तुम कोई दृश्य, किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो. इसी तरह मन कुछ सूंघने, स्वाद लेने, सुनने अथवा स्पर्श करने के लिए अथवा पढ़े-सुने विचार की और भागता रहता है. ऐसे किसी भी अनुभव की चाह तुम्हें वर्तमान क्षण में नहीं रहने देती है.
कुछ क्षण के लिए ही सही, तुम कहो कि चाहे कितना भी सुंदर दृश्य क्यों न हो, मेरी उसे देखने में कोई रूचि नहीं, कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, अभी समय नहीं है और मेरी खाने में अभी कोई रुचि नहीं. कितना ही सुंदर संगीत क्यों न हो, अभी इस समय मुझे सुनने में भी कोई आसक्ति नहीं. कितना भी सुंदर स्पर्श क्यों न हो, मुझे उसे महसूस करने में भी कोई रूचि नहीं है.
चाहे कुछ ही क्षण के लिए ही सही, अपनी इन्द्रियों को विषय वस्तुओं के प्रति इस लालसा और ज्वरता से मुक्त कर लेना ही वैराग्य है.
योगदर्शन में वैराग्य के ‘अपर वैराग्य’ और ‘पर वैराग्य’ दो प्रमुख भेद बतलाए गए हैं.
यतमान वैराग्य – जिसमें विषयों को छोड़ने का प्रयत्न तो रहता है, किन्तु छोड़ नहीं पाता यह यतमान वैराग्य है.
व्यतिरेकी वैराग्य – शब्दादि विषयों में से कुछ का राग तो हट जाए, किन्तु कुछ का न हटे. तब व्यतिरेकी वैराग्य समझना चाहिए.
भारतीय दर्शन में प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द बहुत चर्चित है. हम डूब जाएं और समझ बैठें कि हम उससे भिन्न नहीं हैं, तो यह प्रवृत्ति है. वस्तुत: प्रवृत्त होना शायद उतना घातक नहीं है, जितना प्रवृत्त होने के बाद अपनी मूल सत्ता और स्वरूप का भान न रखना और चित्त के ऐसे स्वामित्व से वंचित हो जाना कि “जब चाहा तब संलग्न और जब चाहा तब विलग्न”. इसे प्रवृत्ति सूचक निवृत्ति की संज्ञा दी जा सकती है. असल में प्रवृत्ति और निवृत्ति के बिना जीवन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती. प्रतिक्षण हम किसी न किसी रूप में प्रवृत्त या निवृत्त होते ही हैं. किन्तु जब हम इतने स्वाधिकार संपन्न होते हैं कि जब चाहा तब प्रवृत्त और जब चाहा तब निवृत्त, तब हमारे उस कर्तव्य में एक और आभा दिखलाई देती है. साधारण प्रवृत्ति के बारे में हम यहां विचार नहीं कर रहे हैं.
वैराग्यशतकम् भर्तृहरि के तीन प्रसिद्ध शतकों (शतकत्रय) में से एक है. इसमें वैराग्य संबंधी सौ श्लोक हैं.
वैराग्यशतकम् में भर्तृहरि ने कितनी गंभीर बात कही है –
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता: तपो न तप्तं वयमेव तप्ता: ||
कालो न यातो वयमेव याता: तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: ||
(अर्थ – भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया. तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए. काल (समय) कहीं नहीं गया, बल्कि हम स्वयं चले गए. इस सभी के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गई (जीर्ण नहीं हुई), बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए.)
इस प्रकार भृतहरि ने यहां संसार की आसारता और वैराग्य के महत्व का प्रतिपादन किया है. इस शतक में काव्य-प्रतिभा और दार्शनिकता का अद्भुत समन्वय किया गया है. इसमें सांसारिक आकर्षणों और भोगों के प्रति उदासीनता के उभरते हुए भावों का चित्रण दिखायी देता है. कवि की तो यही कामना है कि किसी पुण्यमय अरण्य में शिव-शिव का उच्चारण करते हुए उसका समय बीतता जाए.
वैराग्य का मतलब विमुख होना नहीं, बल्कि अपने और पराए, राग और द्वेष से ऊपर उठकर निष्काम और निष्पक्ष सत्य का अनुसंधान करना है. चिंतन करना ही सच्चा वैराग्य है. जिसकी आत्मा में वैराग्य भाव आ जाते हैं, वह निर्भीक, निडर और साहसी बनकर कफन का टुकड़ा भी सिर पर बांधकर जीने मरने की परवाह न करते हुए मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए मैदान में उतरता है. वैराग्य का संबंध वेश पंथ और परंपरा से नहीं, बल्कि विचारों से, अंतर्मन से वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करना वैराग्य है. त्याग, सादगी और साधना वैराग्य का लक्षण है, इसके बिना स्थायी शांति और आत्म कल्याण नहीं हो सकता.
संसार में रहकर व्यक्ति जिन चीजों का उपभोग करता है, उनकी एक कीमत है. इसलिए सांसारिक सुखभोग के अनुरूप व्यक्ति का उतना ही पुण्य, उतना ही तप क्षीण हो जाता है, कट जाता है. इतना सुख आपने भोगा, आपका उतना पुण्य इसमें खप गया. संसार में प्रकृति की, परमात्मा की कप्यूटराइज्ड व्यवस्था है. हम जो कर्म करते हैं, अच्छा-बुरा, श्रेष्ठ-निकृष्ट जो भी करते हैं, वो उस कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्था के तहत नोट हो जाता है. क्योंकि आपने तो कर्म किया, भले ही कैसी भी परिस्थितियों में किया, किन परिस्थितियों में किया, यह माने नहीं रखता और उस कर्म के अनुरूप कर्मफल विधान हम पर अनिवार्य रूप से लग जाता है. हम समझते हैं कि त्याग में हम गंवाते हैं. नहीं, त्याग में हम पाते हैं. आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि त्याग है. इसलिए उच्चतम साधना, श्रेष्ठतम साधना व श्रेष्ठतम अनुशासन, जिनको कहते हैं – वो विवेक और वैराग्य है. विवेक और वैराग्य क्यों है? क्योंकि विवेक और वैराग्य जितना दृढ़ होते हैं, उतना हमारा व्यक्तित्व स्थिर और शांत होता है. इससे हमारे तन और मन में स्थिरता आती है.
नयन मणि कुमार
सहायक अभियंता, गुवाहाटी रिफाइनरी
7002078192