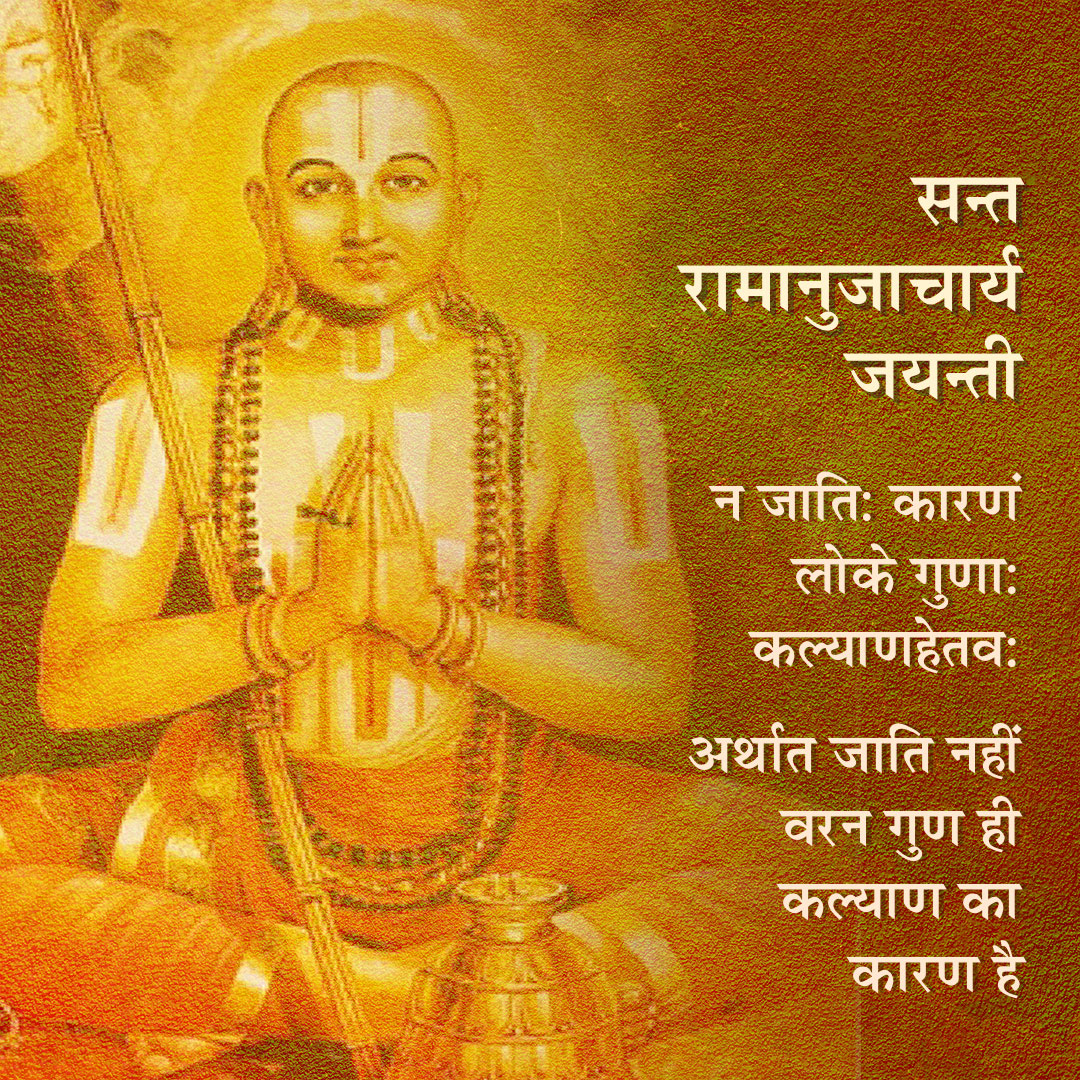आदि शंकराचार्य के दर्शन और सिद्धांतों ने उपनिषदों और वैदिक साहित्य की प्रामाणिकता को पुनर्जीवित किया. वेदों की व्याख्या में शंकराचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं और उन्होंने ‘अद्वैत-वेदांत’ मत स्थापित किया. शंकराचार्य जी की शिक्षाएं पूर्णरूपेण ईश्वरवाद के स्थान पर अधिक अध्यात्मवादी ही थी, रामानुजाचार्य द्वारा उन्हें पुनः ईश्वरीय तत्वों से अभिसिंचित किया गया और उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत (यद्यपि जगत् और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न हैं फिर भी वे ब्रह्म से ही उदभूत हैं) देकर इस कार्य को पूर्ण किया. हिन्दू वैष्णव मत की पुन: प्रतिष्ठा करने वालों में रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है.
रामानुज का जन्म वैशाख, शुक्ल पक्ष, षष्ठी, 1074, विक्रम संवत तदनुसार 1017 ई. में भारत के तमिलनाडु प्रान्त के श्रीपेरम्बुदुर में हुआ था. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, उनके जन्म के समय सूर्य कर्क राशि में था. उनके माता-पिता अशुरी केशव और कांतिमती दोनों कुलीन ब्राह्मण परिवारों से थे. रामानुज ने अपना बचपन पैतृक गांव श्रीपेरम्बुदुर में व्यतीत किया .
8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत (जनेऊ) संस्कार के साथ ही उन्हें वेदों की शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया गया था. बाल्यकाल में ही सब उनकी बुद्धिमत्ता और स्मरणशक्ति के वशीभूत हो गए थे. 16 वर्ष की उम्र में रक्षाम्बा नामक की लड़की से उनका विवाह हुआ था. उन्हें वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दी गई. विवाह के चार माह बाद ही रामानुज के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई. अपने पिता की मृत्यु के उपरांत रामानुज घर के प्रमुख बन गए और उन्होंने विद्वानों और शानदार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पवित्र शहर कांची जाने का निर्णय किया.
कुछ ही समय के पश्चात रामानुज ने अपने घर पर एक छोटा सा विद्यालय खोला और बहुत ही कम समय में उनकी भक्ति और ज्ञान के प्रवचन सुनने के लिए कई लोग उसके पास आने लगे. संत रामानुजाचार्य का जीवनकाल 120 वर्षों का था. उन्होंने विक्रम संवत 1194 अर्थात 1137 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था. श्रीरंगम में अपने निधन से पहले यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य के लिए तीन सन्देश छोड़े थे – वेदांत सूत्रों के भाष्य की रचना करो, आलवारों के भजन संग्रह को संकलित कर ‘पंचम वेद’ के नाम से लोकप्रिय बनाओ और मुनि पराशर के नाम पर किसी विद्वान का नामकरण करो.
रामानुज ने संदेश दिया “जीव, भगवान का एक कण है, इस प्रकार, उसकी स्थिति संपूर्ण की सेवा करने की है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हाथ शरीर का अंग है और इस प्रकार वह शरीर का सेवक है, उसी प्रकार जीव भी परमात्मा का अंश है और इस प्रकार उसकी अवयवात्मक स्थिति सर्वोच्च की सेवा करने की है”. रामानुज के दर्शन को विशिष्टाद्वैत या योग्य अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है.
तदनुसार, यह माना जाता है जीव गुणात्मक रूप से सर्वोच्च के समान और साथ ही साथ मात्रात्मक रूप से भिन्न है. रामानुज का मानना था कि मात्रात्मक अंतर का अर्थ है कि अंश (जीव) सर्वोच्च सत्ता (ईश्वर) पर निर्भर है, लेकिन वह सर्वोच्च नहीं बन सकता.
उनके दर्शन ने घोषित किया कि एक अयोग्य (अस्तित्वहीन) वस्तु का ज्ञान कभी नहीं हो सकता; ज्ञान अनिवार्य रूप से किसी वस्तु की ओर संकेत करता है. जिसके कुछ लक्षण और गुण होते हैं. रामानुज ने कभी भी एक निर्गुण, उदासीन ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि एक ब्रह्म-स्वयं परमदेव, के रूप में स्वीकार किया जो बृहद वास्तविकता का एक गुण है: उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि जीवित वस्तुएं व्यक्तिगत व्यक्तित्व हैं, इसलिए सर्वोच्च सत्ता भी एक व्यक्तित्व है और वही अंतिम व्यक्तित्व है.
रामानुज ने आगे तर्क दिया कि यदि भ्रम सर्वोच्च की पहचान को ढक सकता है, तो वह भ्रम परमात्मा से बड़ा चाहिए. इसलिए उन्होंने बल देकर कहा कि हम सदा व्यक्तिगत व्यक्तित्व हैं और सर्वोच्च सदा सर्वोच्च व्यक्तित्व है, किन्तु हम हमारे परिमित प्रकृति के कारण कभी-कभार भ्रम के अधीन होते हैं. रामानुज ने स्वरूप परिवर्तन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया.
विशिष्टाद्वैत दर्शन की प्रणाली में सर्वोच्च व्यक्तित्व से न तो भौतिक दुनिया और न ही जीवों को स्वतंत्र होने की कल्पना की जाती है. जीव स्वतंत्र इच्छा से संपन्न होने के कारण परमात्मा की एक अलग अभिव्यक्ति हैं, जबकि भौतिक ऊर्जा सीधे सर्वोच्च की इच्छा के तहत प्रकट होती है. जीव की स्वतंत्र इच्छा एक सर्व-महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उस स्वतंत्र इच्छा को ईश्वर और जीव के बीच पारस्परिक संबंधों का मूल सिद्धांत माना जाता है.
रामानुज ने सनातन सेवा के रूप में ईश्वर के साथ जीव के संबंधों को प्रस्तुत किया. रामानुज के अनुसार, जब जीव भक्ति और ईश्वर के प्राकृतिक प्रेम द्वारा एक स्नेही सेवक और उसके स्वामी के बीच सम्बन्धों की भांति भौतिक ऊर्जा द्वारा उत्पन्न भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तब आत्मा वैकुंठ नामक आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करती है. एक बार वैकुंठ संसार में पहुंचने के बाद, आत्मा सर्वोच्च व्यक्ति, नारायण (विष्णु) की अनंत सेवा में संलग्न हो जाती है. यह उदात्त संदेश रामानुज द्वारा प्रतिदिन अपने श्रोताओं को दिया जाता था.
रामानुज की कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई थी. एक दिन जब रामानुज अपने अध्ययन के एकांत में बैठे थे, यमुनाचार्य नामक एक आदरणीय संत भिक्षा के लिए उनके दरवाजे पर आए. रामानुज ने पूर्ण शिष्टाचार का परिचय देते हुए संत का अपने घर में स्वागत किया. रामानुज को पता चला कि यमुना विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर श्री रंगम से थे. उनकी चर्चा के दौरान, रामानुज ने जल्द ही अनुभव किया कि यमुनाचार्य भक्ति शास्त्र के एक योग्य आध्यात्मिक गुरु थे. परमानंद और उल्लास से अभिभूत, रामानुज उनके चरणों में गिर गए और शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा.
यमुना ने तुरंत रामानुज को धरती से ऊपर उठाया, और उन्हें प्रेम से गले लगाते हुए कहा, “मेरे बच्चे, मैं आज भगवान के प्रति आपकी भक्ति को देखकर धन्य हूं. आप नारायण-ईश्वर के व्यक्तित्व की सेवा में हमेशा एक लंबा और फलदायी जीवन जिएं,” रामानुज ने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने गुरु की परिक्रमा की और आशीर्वाद देकर यमुनाचार्य श्री रंगम के लिए प्रस्थान कर गए.
अब रामानुज ने पहले से कहीं अधिक, शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति के सिद्धांत का प्रचार करना आरंभ कर दिया. फिर एक दिन, श्री रंगम से एक दूत आया और रामानुज को सूचित किया कि उनके गुरु बीमार हैं और मृत्यु के कगार पर हैं. रामानुज तुरंत श्री रंगम के लिए प्रस्थान किया, किन्तु समय पर वहां नहीं पहुंच पाए. रामानुज के पहुँचने से कुछ समय पहले, यमुना ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया था और वैकुंठ के आनंदमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे.
कावेरी नदी के तट को पार करके रामानुज उस टापू पर पहुंचे, जिस पर श्री रंगम का मंदिर स्थित था, और सीधे उस स्थान पर गए जहां उनके गुरु मृत पड़े थे. अपने शिष्यों के एक समूह से घिरे, यमुनाचार्य अपनी आँखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनकी भुजाएँ उनके किनारों पर फैली हुई थी, और उनका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कि कोई अनंत सौंदर्य के विचारों में डूबा हुआ हो.
जैसे ही रामानुज ने गुरु के कमरे में प्रवेश किया और अपने गुरु के पास आकर बैठ गए, क्षण भर में सभी का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया. उसकी आँखों में प्यार के आँसू भर आए और वह रो पड़े, उनका हृदय अपने गुरु से बिछड़न से बहुत दुख अनुभव कर रहा था. यमुना का बायां हाथ शांति योग मुद्रा में था, तीन अंगुलियां आगे की ओर बढ़ी हुई थी और अंगूठा और तर्जनी के एक साथ जुड़ा हुआ था. हालाँकि, उनका दाहिना हाथ उनकी तरफ था, लेकिन मुट्ठी में जकड़ा हुआ था. सभी शिष्य अपने गुरु के दाहिने हाथ की स्थिति के बारे में आश्चर्यचकित थे, किन्तु उनमें से कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ सका.
रामानुज ने यह घोषणा करके चुप्पी तोड़ी, “हमारे गुरु-पूज्य यमुनाचार्य की तीन इच्छाएँ हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं. मैं सामान्य रूप से उन अवैयक्तिकता से भ्रमित लोगों की नारायण के कमल के चरणों में समर्पण उन्हें अमृत प्रदान करके रक्षा करूँगा.” जैसे ही रामानुज ने यह कहा, यमुनाचार्य के दाहिने हाथ की एक अंगुली बाहर की ओर निकलकर उठ खड़ी हुई. तब रामानुज ने कहा, “दुनिया के लोगों की भलाई के लिए, मैं वेदांत-सूत्र पर एक टिप्पणी तैयार करूंगा जो सर्वोच्च सत्ता (ईश्वर) को अंतिम वास्तविकता के रूप में स्थापित करेगा.”
इस बात पर, यमुनाचार्य की एक दूसरी उंगली विस्तारित हुई और रामानुज ने बोलना जारी रखा. “और पराशर मुनि को सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने प्राचीन काल में जीवों, जीवित संस्थाओं और ईश्वर-सर्वोच्च व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित किया, मैं इसके लिए अपने एक शिष्य का नाम लूंगा, जिसने पर्याप्त रूप से (अध्यात्म) सीखा है और उनके प्रति समर्पित है.” तब रामानुज चुप हो गए और यमुना के दाहिने हाथ की तीसरी उंगली आगे की ओर उठी. इस चमत्कार को देखकर उपस्थित सभी लोग चकित रह गए और उस दिन से उन सभी ने रामानुज को अपना मार्गदर्शक मान लिया. रामानुज अपने शेष जीवन भर श्री रंगम में रहे और नियत समय में उनके द्वारा तीनों प्रतिज्ञाओं को पूरा किया गया.
यद्यपि उन्होंने एक सफल गृहस्थ के रूप में कई वर्षों तक जीवन यापन किया, किन्तु रामानुज के लिए त्याग का मार्ग स्वीकार करना तय था. अंततः उन्होंने मंदिर में देवता के सामने जाकर, भगवान की सेवा में विशेष रूप से शामिल होने की प्रार्थना करते हुए, गृहस्थ जीवन के त्याग (संन्यास) का त्याग आदेश लिया. उस दिन से रामानुज ने हमेशा अपने माथे पर नारायण का प्रतीक चन्दन लगाना, भगवा वस्त्र धारण करना, और त्यागी के तीन-खंड वाले कर्मियों को अपने जीवन का अंग बना लिया, जो शरीर, मन और शब्दों से भगवान की सेवा का प्रतीक था. रामानुज ने भक्ति के सिद्धांतों को इतनी दृढ़ता से स्थापित किया कि कोई भी उनका विरोध नहीं कर सका. कई महान और विद्वान उन्हें बोलते सुनने के लिए आते थे और वे उनके शिष्य बनते गए.
रामानुज 120 वर्ष की आयु तक श्री रंगम में रहे, नारायण देवता की सेवा की और जो भी उनके पास आया, उन्हें ज्ञान प्रदान किया. एक दिन देवता की पूजा करते हुए, उन्होंने प्रार्थना की, “प्रिय भगवान, जो कुछ भी मैं वेदों के सार को संरक्षित करने के लिए कर सकता हूं, पतित आत्माओं के उत्थान और जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में अपने कमल के चरणों की शरण स्थापित करने के लिए, मेरे पास है, किया. अब मेरा शरीर इस दुनिया में कई वर्षों के बाद थक गया है. कृपया मुझे इस नश्वर दुनिया से विदा लेने और अपने सर्वोच्च निवास में प्रवेश करने की अनुमति दें.”
इस प्रार्थना के बाद रामानुज अपने शिष्यों की सभा में लौट आए और इस दुनिया से चले जाने की अपनी इच्छा की घोषणा की. इस घोषणा ने सबको दु:ख के सागर में धकेल दिया, शिष्यों ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और उनसे अपने साथ रहने का अनुरोध किया. उन्होंने प्रार्थना की “आपके दिव्य रूप के गायब होने की कल्पना करना हमारे लिए असहनीय है, जो सर्वोच्च शोधक है, जो सभी अच्छा है, सभी दुखों का नाश करने वाला और असीमित आनंद का स्रोत है. अपने बच्चों के लिए दया से, कृपया हमारे साथ कुछ समय और रहें.”
शिष्यों के इस अनुरोध पर रामानुज तीन और दिन पृथ्वी पर रहे. रामानुज ने अपने अंतिम निर्देशों को उन लोगों को समझाया जो उनके सबसे निकट और प्रिय थे: “सदैव उसी की संगत में बने रहें और उन आत्माओं की सेवा करें जैसे कि आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक उपदेशक की सेवा करेंगे. वेदों की शिक्षाओं और महान संतों के शब्दों में विश्वास रखें और कभी भी अपनी इंद्रियों के दास न बनें: हमेशा आत्म-साक्षात्कार के तीन महान शत्रुओं : वासना, क्रोध और लोभ. पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें, नारायण की पूजा करें और भगवान के पवित्र नामों को अपने एकमात्र शरण के रूप में उच्चारण करने का आनंद लें.
रामानुज वास्तव में एक महान धर्मविज्ञानी और संत थे. जिनके जीवन और शिक्षाओं का भारत में आस्तिक विचार के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा है. रामानुज ने अतिव्यक्तिपरक विशेषताओं के साथ पूर्ण इकाई के रूप में भगवान का परिचय कराया और भगवान के प्रति समर्पण की परंपरा का आरंभ किया. इससे भविष्य के ईश्वरवादी सुधारकों के लिए द्वार खुल गए, जो समय-समय पर भगवान और उनके साथ अनन्त सेवकों के बीच एक प्रेमपूर्ण संबंध में आत्मा की उच्चतम क्षमता की महत्ता को और सुदृढ़ करेंगे.